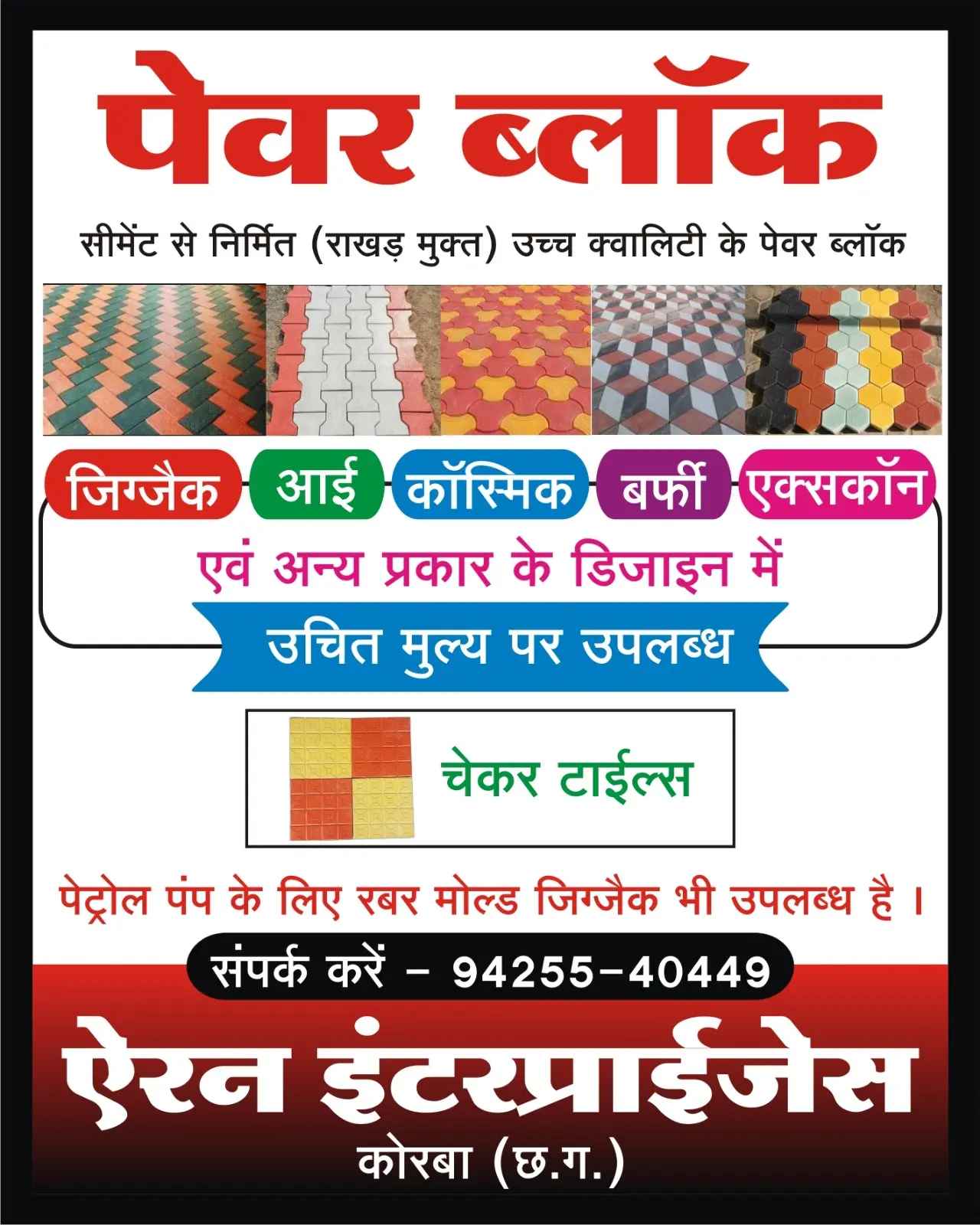जांजगीर- चांपा। जिले के जंगलों में अंधाधुंध पेड़ों की कटाई और लगातार बढ़ती जनसंख्या से पर्यावरण असंतुलित होने लगा है। बढ़ती जनसंख्या, नगरीकरण व उद्योगों के कारण उपजाऊ भूमि की कमी होती जा रही है, वहीं फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं और अपशिष्ट पदार्थ ने पर्यावरण को पूरी तरह से प्रदूषित कर दिया है।जिले की आबादी लगभग 10 लाख है। औद्योगिक इकाइयों के बढऩे से यहां का वातावरण प्रदूषण के चपेट में है। प्रदूषण का असर कम होने के बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे मनुष्य सहित पेड़ पौधे व जीव-जन्तु भी प्रभावित हो रहे हैं। औद्योगिकरण व जनसंख्या वृद्धि के चलते पिछले एक दशक में जिले के भू-जल स्तर में कापुी गिरावट आई है।
कारखानों की चिमनियों व वाहनों के धुएं से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इन धुओं के कारण तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है, वहीं वाहनों में उपयोग होने वाले डीजल-पेट्रोल में शीशा मिले होने के कारण धुएं से कार्बन डाई आक्साइड, कार्बन मोनो आक्साइड व डाई ऑक्सिन जैसे विषैली गैस निकलती है। लोगों के शरीर को सीधे नुकसान हो रहा है। पालीथीन भी धरती के लिए घातक है। इससे जमीन की उर्वरा क्षमता में कमी आती है। वहीं जलीय जंतु व पालतू जानवर इसे खाकर असमय मौत के मुंह में चले जाते हैं।
पालीथीन के खतरे से बचने जूट व कागज के थैले का उपयोग होना चाहिए। इसी तरह मोटर गाडिय़ों के सायरन, फैक्ट्रियों के कलपुर्जो का शोर व मोबाइल टॉवर से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे लोगों के लिए कापुी हानिकारक है। इस प्रभाव से लोग बहरेपन का शिकार होते जा रहे हैं और याददाश्त में भी कमी आती जा रही है। इसके अलावा लगातार बढ़ती जनसंख्या की पर्यावरण असंतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका है। बढ़ती जनसंख्या के कारण लगातार उपजाऊ भूमि का रकबा घट रहा है। दूसरी ओर वनों की धड़ल्ले से कटाई व पौधरोपण के प्रति लोगों की उदासीनता से वातावरण प्रदूषण के चपेट में आ गया है। लोगों की भौतिक जरुरतें भी बढ़ रही है।
नदियों पर मंडरा रहा संकट
औद्योगिक इकाइयों द्वारा सिंचाई विभाग से किए गए अनुबंध से ज्यादा नदी का पानी उपयोग किया जा रहा है, जिसके चलते गर्मी की शुरुआत से ही बोराई और माण्ड नदी का पानी सूख जाता है। वहीं हसदेव और महानदी का जल स्तर भी अब गर्मियों में कम हो जा रहा है। जिसके चलते नदी तट पर बसे गांव के लोगों को निस्तार के लिए परेशान होना पड़ता है।
कुओं की उपेक्षा
निस्तारी के लिए हैण्डपंप व नलों पर निर्भरता ने कुओं के रखरखाव के लिए लोगों को उदासीन बना दिया है। जिले के शहर सहित गांवों के बड़े कुएं कूड़ेदान में तब्दील होते जा रहे हैं। वहीं अब नए कुएं नहीं खोदे जा रहे हैं। घरों के तमाम कूड़े-करकट तालाब किनारे पुेंक दिए जाते हैं और नालियों के गंदे पानी को तालाबों में छोड़ दिया जाता है। जिले के अधिकांश तालाबों की हालत खराब है। गंदगी से पटने के कारण अब लोगों ने तालाब में निस्तार करना कम कर दिया है। कुओं के पाट दिए जाने से जलस्तर भी नीचे जा रहा है। लोगों को भावी पीढ़ी के लिए जल बचाने की कोई चिंता नहीं है।
लगातार कट रहे जंगल
बलौदा ब्लॉक के कई गांव जंगल के आसपास बसे हैं। कुछ वर्ष पहले खिसोरा, पंतोरा, बेलटुकरी, कण्डरा, चारपारा, सोनगुढ़ा सहित लगभग सैकड़ों गांवों के आसपास बड़ी संख्या में साल, सागौन, बीजा, तेंदू, घावड़ा, तिन्सा,हल्दू, आंवला, चार, बांस के पेड़ थे। जिनसें फल, फूल व लगभग ढ़ाई सौ प्रजाति की औषधियां मिलती थी, लेकिन लकड़ी चोरों द्वारा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से जिले के कई जंगल उजड़ गए। जिले में मात्र 4 प्रतिशत वन हैं। टावर लाइन ले जाने, सडक़ निर्माण तथा जलाऊ लकड़ी व फर्नीचर के लिए पेड़ों को काटे जाने से जंगल का दायरा सिमट रहा है।
नहीं बन रहे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम
जिले के गांवों व शहरों में मकान निर्माण धड़ल्ले से चल रहा है। हर साल सैकड़ों मकान बन रहे हैं। लगातार मकान बनने से जल संकट गहराने लगा है। वाटर हार्वेस्टिग विधि काफी पुरानी है, जिससे वर्षा के जल का पूरी तरह सदुपयोग किया जा सकता है, लेकिन लोग इसके प्रति उदासीन है और प्रशासन भी इसे गंभीरता से नहीं ले रहा है। जिसके चलते हर साल गर्मी में पेयजल की समस्या गहराने लगती है।
पर्यावरण को लेकर जागरूक नहीं लोग
जिले के अधिकांश गांव व शहर गर्मी की शुरुआत से ही जल संकट के भयंकर दौर से गुजर रहे हैं। यहां के लोगों में पौधरोपण करने व प्राकृतिक जल स्त्रोत को सुरक्षित रखने के लिए जागरुकता की कमी है, वहीं प्रशासन द्वारा लोगों को जागरुक करने के प्रयास भी नहीं किए जा रहे है। ऐसे में समय रहते यदि लोगों में जागरुकता नहीं आती है तो आने वाले समय में पर्यावरण पूरी तरह से प्रदूषण के चपेट में आ जाएगा।
पढ़ाई हो व्यवहारिक
प्रदूषण नियंत्रण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल और कालेज के पाठ्यक्रमों में पर्यावरण अध्ययन को शामिल करने का निर्देश दिया है, लेकिन राज्य शासन द्वारा स्कूल कालेजों में लागू पाठ्यक्रम पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से पर्याप्त नहीं है। इसमें केवल जल प्रदूषण वायु, ध्वनि व मृदा प्रदूषण के कारण निदान आदि का ही अध्ययन किया जाता है। जबकि पर्यावरण अध्ययन को सैद्घांतिक के बजाय व्यवहारिक किए जाने की आवश्यकता है। इसमें छात्रों को पौधे लगवाने व उनकी देखरेख के लिए प्रेरित करने का प्रावधान हो। वहीं किसानों को खेत व खाली जमीन पर पेड़ लगाने व उसकी सुरक्षा करने पर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।